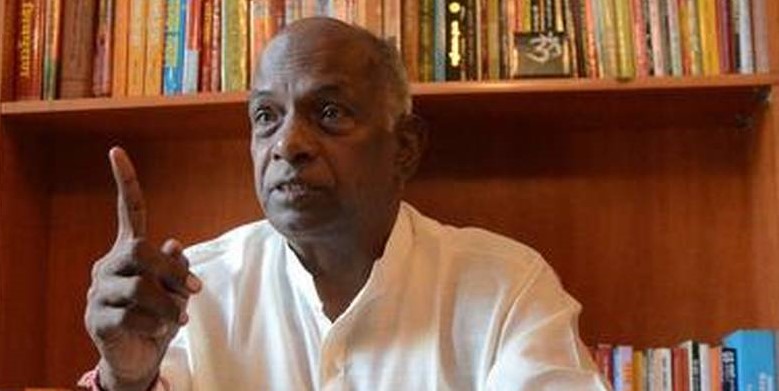 1947 में अंग्रेजों ने भारत की आजादी को केवल ‘सत्ता का हस्तांतरण कहा। अफसोस है कि भारतीय नेतृत्व ने भी यही माना, समझा और समझाया। यह भी हकीकत है कि आजादी आने से पहले महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से इस प्रश्न पर संवाद कायम करना चाहा ताकि स्वाधीन भारत की भावी रचना का खाका बनाया जा सके। लेकिन, इसे उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी ने गैरजरूरी समझा। इस कारण वे सारी मान्यताएं, धारणाएं और शासकीय व्यवस्थाएं पूर्ववत चलती रहीं जिनकी नींव अंग्रेजों ने डाली थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले बाहरी लोग हम पर शासन करते थे लेकिन 1947 के बाद हमारे चुने हुए लोग हम पर शासन करने लगे। इससे अधिक 1947 में कुछ भी नहीं हुआ।
1947 में अंग्रेजों ने भारत की आजादी को केवल ‘सत्ता का हस्तांतरण कहा। अफसोस है कि भारतीय नेतृत्व ने भी यही माना, समझा और समझाया। यह भी हकीकत है कि आजादी आने से पहले महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से इस प्रश्न पर संवाद कायम करना चाहा ताकि स्वाधीन भारत की भावी रचना का खाका बनाया जा सके। लेकिन, इसे उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी ने गैरजरूरी समझा। इस कारण वे सारी मान्यताएं, धारणाएं और शासकीय व्यवस्थाएं पूर्ववत चलती रहीं जिनकी नींव अंग्रेजों ने डाली थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले बाहरी लोग हम पर शासन करते थे लेकिन 1947 के बाद हमारे चुने हुए लोग हम पर शासन करने लगे। इससे अधिक 1947 में कुछ भी नहीं हुआ।
अंग्रेज से मुक्त होने के बाद भारत को अपनी मेधा, अपनी प्रतिभा के साथ दुनिया में अपनी भूमिका अदा करने के लिए जिस आत्मविश्वास से खड़ा होना था, वह सही ढंग से नहीं हो पाया। भारत का आम आदमी, उसका हित और उसका स्वभाव, भारत के अभिजात्य वर्ग के हित और स्वभाव से कट गया।
भारत की पारंपरिक व्यवस्था में समाज की प्रधानता थी। इसलिए यह देश समाज की अदरूनी ताकत और सामाजिक पूंजी के आधार पर चलता था। लेकिन, भारत में जो राज्य व्यवस्था क्रमशः लागू की गयी उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे राज्य व्यवस्था ने समाज को चलाने का ठेका ले रखा है। जिसके कारण यह सोच बनती चली गयी कि सब कुछ राज्य करेगा। जबकि वास्तविकता यह है कि राज्य कभी भी बहुत कुछ करने की स्थिति में था ही नहीं।
वास्तव में भारत चलता था अपनी ‘सामाजिक पूंजी’ और सांस्कृतिक परंपरा के बल पर। भारत के सामाजिक अग्रदूतों का इस सामाजिक जीवन में बहुत योगदान रहा है। उनका अपना एक प्रभाव होता था जिसका लाभ समाज को मिलता था। यहां इसी कड़ी में एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि 19वीं सदी में जहां एक ओर प्रशासकीय स्तर पर यूरोपीय मान्यताओं को लागू किया जा रहा था तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक स्तर पर भारत नई अंगड़ाई भी ले रहा था। ये दोनों घटनाएं साथ-साथ हो रही थीं।
इन सामाजिक अग्रदूतों में एक धारा रामकृष्ण परमहंस की निकली जो अपनी तरह से भारत के नवोत्थान के लिए काम कर रही थी। एक धारा लोकमान्य तिलक की निकली जो अपने तरीके से काम कर रही थी। इसी बीच स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी के रूप में एक महामानव का उदय हुआ। उन्होंने अंग्रेजों के प्रशासन से ही मुक्ति की बात ही नहीं सोची, बल्कि भारतीयता के आधार पर प्रशासन की एक प्राथमिक रूपरेखा भी तैयार की। इसी काल में सुभाष चंद्र बोस का संघर्ष था तो डा. हेडगेवार का बहुमूल्य रचना-संसार और भारत की आत्मप्रतिष्ठा का संघर्ष भी है। ऐसे बहुत से लोग विभिन्न स्तरों पर मानो भारत के पुनर्जागरण के लिए काम कर रहे थे।
1947 में सत्ता के हस्तांतरण के बाद सामाजिक अग्रदूतों या आंदोलनों के साथ राज्य ने कोई तादात्म्य बिठाने की कोशिश नहीं की। इसलिए धीरे-धीरे राज्य और समाज के बीच दूरी बढ़ती चली गयी। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि तिलक द्वारा जन-एकत्रीकरण के लिए शुरू किए गए गणेश-उत्सव को ‘कम्युनिटी’ विशेष का करार दे दिया गया। कल्पना करिए कि आज के समय में भी क्या गांधी जी ‘रघुपति राघव राजाराम’ गाकर सांप्रदायिक होने से बच पाते। ऐसी स्थिति इसलिए निर्माण हुई है क्योंकि राज्य समाज के चलने की मानसिकता से निकल नहीं पा रहा है। इसलिए वह अपनी समझ और सुविधानुसार कायदे-कानून निर्धारण करता है। राज्य ने जो कार्य निर्धारण किए, जो नियमावली बनायी, उससे देश की ऊर्जा, देश की प्रतिभा का उपयोग देश के विकास में पूरी तरह नहीं हो पा रहा है। देश और समाज अपने हिसाब से चल रहा है, जबकि राज्य उसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करने में पूरी तरह से लगा हुआ है।
स्वाधीन भारत में राज्य ने अपने समस्त नियमों-कानूनों का आधार संविधान को बनाया है। इस संविधान के निर्माण में भी भारत एक राष्ट्र है, एक जन है, एक संस्कृति है, इस मूलभूत आस्था का प्रकटीकरण पूरी ताकत से नहीं दिखता। लगता है इसमें कुछ कसर सी रह गयी। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जिस राज्य को समाज की आवश्यकता तथा जन की इच्छा के अनुरूप कार्य करना चाहिए, वह नहीं कर पा रहा है। दुनिया के कुछ देशों की ‘अच्छी बातों’ को लेकर संविधान पूरा कर लिया गया, लेकिन वे ‘अच्छी बातें’ या ‘अच्छी व्यवस्था’ इस देश के लिए कब और कितनी आवश्यक या अनुकूल हैं, लगता है इस पर समग्रता से विचार नहीं किया गया। सच्चाई तो यह है कि आजाद भारत का संविधान 1935 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भारत सरकार अधिनियम का ही संशोधित विस्तार लगता है।
संक्षेप में कहें तो 1947 में हम अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन से तो मुक्त हो गए। लेकिन हम मानसिक रूप से उनके गुलाम बने रहे। उन्होंने अपने शासनकाल में हमारे अंदर जो हीनभावना भरी थी, वह कहीं न कहीं आज भी कायम है। हमारे नेताओं को यह विश्वास है कि यदि देश को गरीबी और दरिद्रता से मुक्ति दिलानी है तो हमे अंग्रेजों के दिखाए रास्ते पर ही चलना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, न्याय व्यवस्था एवं विकास के नाम पर हमारे देश में जो कुछ हो रहा है, उसमें भारतीय परंपराओं एवं यहां की आवश्यकताओं की समझ नहीं दिखाई देती। बल्कि सभी जगह औपनिवेशिक सोच एवं तौर-तरीकों की ही झलक देखने को मिलती है। इसके परिणामस्वरूप पारंपरिक ग्रामीण समाज का एक ओर जहां पतन हो रहा है वहीं शहरीकरण, बाजारीकरण और केंद्रीयकरण जैसी अमंगलकारी व्यवस्थाएं और मजबूत होती जा रही हैं। परिवार, गांव, इलाका, देश, समाज आदि इकाईयों के साथ व्यक्ति के मानस और सोच को संश्लेषित करने की बजाय व्यक्ति को एकाकी समझकर और राज्य को ही संचालन विधि का सर्वस्व मानकर नीतियां बनाई जा रही हैं। येन-केन प्रकारेण अर्थोपार्जन को सुख का आधार मानकर अमर्यादित प्रयास को उचित ठहराया जा रहा है।
इसे हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि देश के संभ्रांत लोगों का एक बड़ा वर्ग विदेशियों की दूसरे-तीसरे दर्जे की कार्बन कापी बनकर जिंदगी जीने मं अपनी सार्थकता अनुभव कर रहा है। इस वर्ग की जड़ें कंपनी राज के दौरान प्रभावी हो चुके उस भारतीय समुदाय में छिपी हैं जो अंग्रेजी को अंधकार दूर करने का जरिया मानता था। अंग्रेजी जानने की ललक पालता था और प्रशासन में हिस्सेदारी उसकी सबसे बड़ी आकांक्षा होती थी। कंपनी राज के दौरान बोया गया वह बीज वटवृक्ष हो गया है। उसका प्रभाव आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में है। मध्य वर्ग उसकी नकल करता है। अंग्रेजीयत के वशीभूत, साधन सम्पन्न एवं बोलने में अत्यंत प्रखर भारत के इस संभ्रांत वर्ग का भारत की भूमि, सभ्यता एवं लोगों के प्रति उपेक्षा भाव है। इसे भारत के भूगोल-इतिहास में कुछ विशेष मूल्यवान नजर नहीं आता।
भारतीय सभ्यता एवं भारत के लोगों के प्रति निर्मम उपेक्षा का यह भाव उस शिक्षा पद्धति का परिणाम है जो ब्रिटिश शासकों ने खासतौर से भारत के लोगों को भ्रमित करने के उद्देश्य से रची थी और जिसे हम अभी तक बदल नहीं पाये हैं। शिक्षित लोगों में अपने देश एवं अपने लोगों के प्रति उपेक्षा एवं वैमनस्य का भाव उत्पन्न करना इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। इस कार्य में अंग्रेज कदाचित अपनी अपेक्षाओं से भी अधिक सफल हुए।
भारत के शिक्षित-संभ्रांत लोगों ने अंग्रेजों द्वारा स्थापित वैचारिक-बौद्धिक संरचना और उस पर आधारित शिक्षा पद्धति मे निहित पूर्वाग्रहों एवं मूल्यों को न केवल अब तक संजोए रखा है, बल्कि उसे इतनी गहराई तक आत्मसात कर लिया है कि इसमें तनिक भी परिवर्तन के प्रयास का वे घोर विरोध करते हैं। इस विरोध में वर्तमान प्रचार तंत्र पूरी रह इनका साथ देता है। सक्षम-संभ्रांत इन लोगों में अपने देश एवं अपनी सभ्यता के मूलतत्व के प्रति निर्बाध समर्पण के अभाव में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के प्रयास सशक्त नहीं हो पा रहे हैं। हम अपनी समस्त शक्ति एवं समस्त साधनों का नियोजन राष्ट्रीय गौरव की पुनः प्राप्ति के एकमेव लक्ष्य हेतु नहीं कर पा रहे हैं।
संभ्रांत लोगों के इस वर्ग में पश्चिमी सभ्यता के प्रति आसक्ति और भारतीय सभ्यता के प्रति उपेक्षा का जो भाव है, वह अपने आप नहीं मिटने वाला है। इस काम को करने का दमखम किसी और के पास नहीं बल्कि भारत के उन लोगों के पास ही है, जो आज भी भारतीय सभ्यता से दूर नहीं हुए हैं। जब अंग्रेजियत में डूबे सक्षम संभ्रांत लोग इन लोगों की बढ़ती शक्ति और क्षमताओं को समझेंगे तभी उनके मन में भी भारतीय सभ्यता के प्रति आदर का भाव उत्पन्न होगा।
‘व्यवस्था परिवर्तन की राह’ पुस्तक से साभार
