
इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में दो बार देश में इमरजेंसी लगवाई। दूसरी इमरजेंसी 1975 की है। उस काल में एक तरफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तानाशाही थी तो दूसरी तरफ लोकतंत्र की आवाज बने लोकनायक जयप्रकाश नारायण (जेपी) थे। जे.पी. मौलिक चित्त के मालिक थे। वे लोकतंत्र के सजग प्रहरी थे। इंदिरा गांधी सत्ता लोलुप थी। अक्सर हर युवा क्रांतिकारी होता है। लेकिन जेपी आजीवन क्रांतिकारी थे। एक क्रांतिकारी सत्ता के दमन की परवाह नहीं करता। इंदिरा गांधी अपनी सत्ता के लिए दमन नीति को अपनाने और उसे उचित ठहराने के लिए असत्य का भी सहारा लेती थीं। जेपी सत्य के साथ खड़े थे। 1975 की इमरजेंसी सत्य और असत्य के संघर्ष की कहानी है। जिसमें अंततः सत्य जीता।
सत्य–असत्य का संघर्ष अनादिकाल से होता आया है। इमरजेंसी में जो इंदिरा गांधी के साथ थे वे भयवश थे। जेपी के साथ जो थे, वे अभय थे। इमरजेंसी में कांग्रेस एक दरबारी पार्टी हो गई थी लेकिन जिनका भी अपना विवेक बचा हुआ था, वे इमरजेंसी को भारत के हितों पर मार्मिक चोट मानते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था, जिसे इतिहास में बड़े आदर के साथ कामराज के नाम से जाना जाता है। वे पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री काल में इसलिए मशहूर हुए क्योंकि कांग्रेस में नया जीवन फूंकने के लिए जो चर्चित योजना बनी और घोषित हुई, उसे कामराज योजना कहते हैं। के. कामराज तमिलनाडु से थे। कांग्रेस के बड़े नेता थे। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में उनकी प्रमुख भूमिका थी। इमरजेंसी के घोषित होने के दो दिनों बाद तमिलनाडु के तिरूवल्लूर में उन्होंने एक भाषण दिया। वह याद करने लायक है, ‘मुझे लगता है कि एक जंगल में मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर छोड़ दिया गया है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि आपातकाल के परिणाम क्या होंगे? क्या कोई यह कल्पना भी कर सकता था कि इस प्रकार से आपातकाल की घोषणा होगी। 1971 के चुनाव में मैंने अपनी आशंका व्यक्त की थी कि लोकतंत्र को खतरा है। करूणानिधि व श्रीमती गांधी, जिन दोनों का उस समय गठबंधन था, ने मेरी खिल्ली उड़ाई थी। मैंने 1971 में जो कहा था वह 1975 में घटित हो रहा है…।’
 ऐसी आशंका प्रकट करने वाले कामराज अकेले राजनेता नहीं थे। 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी ही आशंका जेपी ने भी अपने पत्र में प्रकट की थी। उन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था। तब जेपी के लिए इंदिरा गांधी ‘इंदू’ थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जेपी बड़ा भाई मानते थे। इस नाते उनका इंदिरा गांधी से ‘चाचा–भतीजी’ का संबंध बना हुआ था। उसी संबंध का वास्ता देकर जेपी ने इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखा वह एक परामर्श था और उसमें चेतावनी भी थी। वह पत्र है, ‘तुमको देश की जनता की सेवा का अपूर्व अवसर मिला है। मुझे आशा है कि तुम गंभीरता से सोच–विचारकर आज की चुनौतियों का सामना धीरज व विनम्रता से करोगी… राष्ट्रपति–निर्वाचन के समय का तुम्हारा आचरण मुझे पसंद नहीं आया था, यद्यपि मैं जानता हूं कि तब तुम्हारे राजनीतिक जीवन–मरण का प्रश्न था। अब जब तुम्हें निर्द्वन्द्व सत्ता मिली है मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वह तुम्हारे विवेक को शुद्ध रखे।’
ऐसी आशंका प्रकट करने वाले कामराज अकेले राजनेता नहीं थे। 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी ही आशंका जेपी ने भी अपने पत्र में प्रकट की थी। उन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था। तब जेपी के लिए इंदिरा गांधी ‘इंदू’ थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जेपी बड़ा भाई मानते थे। इस नाते उनका इंदिरा गांधी से ‘चाचा–भतीजी’ का संबंध बना हुआ था। उसी संबंध का वास्ता देकर जेपी ने इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखा वह एक परामर्श था और उसमें चेतावनी भी थी। वह पत्र है, ‘तुमको देश की जनता की सेवा का अपूर्व अवसर मिला है। मुझे आशा है कि तुम गंभीरता से सोच–विचारकर आज की चुनौतियों का सामना धीरज व विनम्रता से करोगी… राष्ट्रपति–निर्वाचन के समय का तुम्हारा आचरण मुझे पसंद नहीं आया था, यद्यपि मैं जानता हूं कि तब तुम्हारे राजनीतिक जीवन–मरण का प्रश्न था। अब जब तुम्हें निर्द्वन्द्व सत्ता मिली है मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वह तुम्हारे विवेक को शुद्ध रखे।’
इंदिरा गांधी को वह पत्र तीर की तरह चुभा। जो जवाब दिया वह उनके दृष्टिकोण का परिचायक है। उनके जवाब में तानाशाही की बू है। ‘राष्ट्रपति चुनाव के समय का मेरा आचरण आपको पसंद नहीं आया पर आपने यह स्वीकार किया कि मेरे राजनीतिक जीवन के लिए यह आवश्यक था। यह पढ़कर मुझे दुख हुआ और विशेषकर यह जानकर कि आप मुझे कितना कम जानते, समझते हैं। मैंने कभी राजनीतिक या किसी अन्य प्रकार के अस्तित्व की चिंता नहीं की। उस समय जो प्रश्न था वह मेरे भविष्य का नहीं, पर कांग्रेस पार्टी और इसीलिए देश के भविष्य का था। मेरी अपनी कोई ऐसी आकांक्षा नहीं है जो मुझे अपने सिद्धांतों से विचलित कर सके।’ इस पत्र में वे कांग्रेस और देश का स्वयं को पर्याय बता रही हैं। यही तानाशाही मानसिकता है।
इसका जेपी ने शालीन पर कड़ा उत्तर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘मेरे उस वाक्य का तुमने बिलकुल गलत अर्थ लगाया। मैंने कभी यह नहीं माना कि तुम्हारा वह आचरण तुम्हारे राजनीतिक जीवन के लिए आवश्यक था। मेरा यह अभिप्राय नहीं था। जिस आचरण को मैं ठीक नहीं समझता, उसे मैं आवश्यक कैसे मान सकता हूं? मेरा तात्पर्य तो इससे बिलकुल विपरीत था, वह यह था कि यह जानते हुए भी कि वह समय राजनीतिक जीवन में तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, मैंने तुम्हारा आचरण पसंद नहीं किया था…यह ठीक है कि राजनीतिक नेता के रूप में मैं तुम्हें बहुत कम जानता हूं। मैं तो तुम्हें दूसरे रूप में ही जानता रहा हूं और आज भी तुम्हें उसी रूप में देखता हूं, व तुम्हारी सफलताओं पर प्रसन्न होता हूं, …लेकिन राजनीति का मेरा भी लंबा अनुभव है और राजनीति से अलग होने के बाद भी मैं बड़ी तटस्थता से सब कुछ देखता समझता रहा हूं। दलों की फूट का भी मुझे काफी अनुभव है। इसी के आधार पर यह कहने की धृष्टता करता हूं कि जब भी किसी दल में फूट पड़ती है तो दोनों तरफ के नेताओं का दावा यही होता है कि झगड़ा सिद्धांत और नीति का है, कोई भी यह नहीं कहता कि झगड़ा व्यक्तिगत सत्ता या पद का है। हर फूट में थोड़ा बहुत विचार का मतभेद हो सकता है…लेकिन उसमें नेतृत्व का, पद का झगड़ा भी कम नहीं होता…और अंत में इतना और कह दूं कि अब तक कई अवसरों पर तुम्हारे राजनीतिक आचरण को मैंने पसंद नहीं किया है पर सार्वजनिक रूप से कभी तुम्हारे विरूद्ध कुछ नहीं कहा…यह सब इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि तुम्हें खुश करना चाहता हूं या अपने लिए तुमसे कुछ अपेक्षा करता हूं बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है कि तुम भी मुझे कम जानती हो।’
राजनीतिक जीवन के लिए आवश्यक था। मेरा यह अभिप्राय नहीं था। जिस आचरण को मैं ठीक नहीं समझता, उसे मैं आवश्यक कैसे मान सकता हूं? मेरा तात्पर्य तो इससे बिलकुल विपरीत था, वह यह था कि यह जानते हुए भी कि वह समय राजनीतिक जीवन में तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, मैंने तुम्हारा आचरण पसंद नहीं किया था…यह ठीक है कि राजनीतिक नेता के रूप में मैं तुम्हें बहुत कम जानता हूं। मैं तो तुम्हें दूसरे रूप में ही जानता रहा हूं और आज भी तुम्हें उसी रूप में देखता हूं, व तुम्हारी सफलताओं पर प्रसन्न होता हूं, …लेकिन राजनीति का मेरा भी लंबा अनुभव है और राजनीति से अलग होने के बाद भी मैं बड़ी तटस्थता से सब कुछ देखता समझता रहा हूं। दलों की फूट का भी मुझे काफी अनुभव है। इसी के आधार पर यह कहने की धृष्टता करता हूं कि जब भी किसी दल में फूट पड़ती है तो दोनों तरफ के नेताओं का दावा यही होता है कि झगड़ा सिद्धांत और नीति का है, कोई भी यह नहीं कहता कि झगड़ा व्यक्तिगत सत्ता या पद का है। हर फूट में थोड़ा बहुत विचार का मतभेद हो सकता है…लेकिन उसमें नेतृत्व का, पद का झगड़ा भी कम नहीं होता…और अंत में इतना और कह दूं कि अब तक कई अवसरों पर तुम्हारे राजनीतिक आचरण को मैंने पसंद नहीं किया है पर सार्वजनिक रूप से कभी तुम्हारे विरूद्ध कुछ नहीं कहा…यह सब इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि तुम्हें खुश करना चाहता हूं या अपने लिए तुमसे कुछ अपेक्षा करता हूं बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है कि तुम भी मुझे कम जानती हो।’
इस पत्र में जेपी का दृष्टिकोण सकारात्मक है। लेकिन इंदिरा गांधी ने न तब और न उस समय उन्हें समझने का प्रयास किया जब बिहार आंदोलन में संवाद का एक अवसर आया। उसका वर्णन कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता श्याम नंदन मिश्र ने अपने संस्मरण में किया है। उनके संस्मरण का शीर्षक है, ‘जेपी आंदोलन की कुछ स्मृतियां।’ यह संस्मरण उन्होंने जेपी के शताब्दी वर्ष में लिखा। वह पत्र–पत्रिकाओं में उस समय छपा था। उन्हीं दिनों जब मैं श्याम बाबू से मिलने गया तो उन्होंने अपने लेख की एक प्रति दी। उनके लेख में जेपी और इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व का एक मूल्यांकन भी है। उन्होंने लिखा है कि ‘बिहार के जन आंदोलन में स्वातंत्र्य संग्राम की कुछ झलक थी। इसके नेता जयप्रकाश नारायण चाहे कितने अवतारों में प्रकट होते रहे हों किंतु उनके व्यक्तित्व में गांधी विरासत के सत्य की ज्योति अंतिम क्षणों तक बनी रही। यही कारण था कि वे विरोधी को दुश्मन न मानकर उससे संवाद बनाए रखने के लिए तैयार रहते थे।’
उन्होंने लिखा कि ‘बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम कि 1974 के आंदोलन में कभी जयप्रकाश–इंदिरा वार्ता का भी प्रकरण आया था। अगर विधान सभा विघटन के प्रश्न का कोई समाधान निकल गया होता तो परिस्थिति ने आगे इतना भयंकर रूप न धारण किया होता। यह वार्ता–प्रकरण चूंकि मुख्यतः मेरे अभिक्रम से आया था मैं इसके प्रकाशन से बराबर कतराता रहा। यह भय था कि इसे मेरी कीर्ति–गाथा समझा जाएगा।’ वार्ता का सुझाव उन्हें राजा दिनेश सिंह ने दिया था। उनमें गहरी मित्रता थी। श्याम नंदन मिश्र लोकसभा के प्रखर नेताओं में एक थे। उन्होंने अपने लेख में बताया है कि कैसे यह शुरूआत हुई।
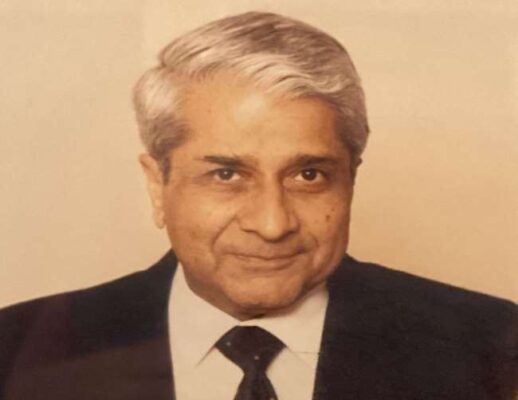 एक दिन जब राजा साहब (दिनेश सिंह) ने मुझसे कहा, ‘श्याम बाबू इंदिरा जी से मिलिएगा?’ ‘वे मिलना चाहतीं हैं।’ ‘मैंने हां कर दी।’ उन्होंने लिखा है, ‘मुलाकात साउथ ब्लाक में हुई। समय दोपहर बाद 4-5 बजे का रहा होगा। जब बातचीत शुरू हुई तो मैंने कहा कि कोई हल तो निकालना ही चाहिए। अगर आप चाहेंगी तो जरूर निकलेगा। आखिर कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है। लेकिन इस संदर्भ में मेरे नेता जयप्रकाश बाबू हैं, उनका जो फैसला होगा उसी पर मैं चलूंगा। पहले अपना विचार उनकी आंखों में देखे बिना पूरी सफाई से रख दूंगा। फिर मैंने मजाक के लहजे में पूछा कि क्या आपने अपने इर्दगिर्द अपने सहयोगियों को ऐसी आजादी दे रखी है? इस पर वे मुस्कुराईं।’
एक दिन जब राजा साहब (दिनेश सिंह) ने मुझसे कहा, ‘श्याम बाबू इंदिरा जी से मिलिएगा?’ ‘वे मिलना चाहतीं हैं।’ ‘मैंने हां कर दी।’ उन्होंने लिखा है, ‘मुलाकात साउथ ब्लाक में हुई। समय दोपहर बाद 4-5 बजे का रहा होगा। जब बातचीत शुरू हुई तो मैंने कहा कि कोई हल तो निकालना ही चाहिए। अगर आप चाहेंगी तो जरूर निकलेगा। आखिर कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है। लेकिन इस संदर्भ में मेरे नेता जयप्रकाश बाबू हैं, उनका जो फैसला होगा उसी पर मैं चलूंगा। पहले अपना विचार उनकी आंखों में देखे बिना पूरी सफाई से रख दूंगा। फिर मैंने मजाक के लहजे में पूछा कि क्या आपने अपने इर्दगिर्द अपने सहयोगियों को ऐसी आजादी दे रखी है? इस पर वे मुस्कुराईं।’
उनके लेख का यह अंश जेपी के व्यक्तित्व की विशेषताओं से परिचित कराता है। ‘जब जयप्रकाश बाबू के उठाए गए मुद्दों पर चर्चा चली तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपकी जगह मैं होता तो जेपी को थका देता। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा– वह बड़ा थारो आदमी है। किसी विषय को अपने हाथ में लेता है तो उसकी पूरी छानबीन में लग जाता है, खुद भी और विशेषज्ञों की सहायता लेकर भी। इसलिए शिक्षा में सुधार, चुनाव प्रणाली में परिवर्तन, भ्रष्टाचार उन्मूलन आदि विषयों को उनके सुपूर्द कर देता और कहता कि आप सुधार का मसविदा तैयार कराएं। इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, इस पर दो राय तो है नहीं।’ इस वर्णन के बाद उन्होंने लिखा है कि ‘मैंने इंदिरा जी से कहा कि जब मैं जेपी से बात करूं तो आपका कोई विश्वासी व्यक्ति भी वहां रहे।’ उन्होंने लिखा है कि इससे इंदिरा जी थोड़ी परेशानी में आई। उन्होंने मुझसे कहा कि आप ही नाम बताइए। मैंने राजा दिनेश सिंह का नाम लिया। पंडित मोती लाल नेहरू के जमाने से ही काला कांकर राज परिवार और नेहरू परिवार का गहरा संबंध चला आ रहा था। उन्होंने लिखा है कि ‘इंदिरा जी ने राजा दिनेश सिंह के नाम की स्वीकृति दे दी।’
बिहार आंदोलन में वह बड़ा निर्णायक समय था। श्याम नंदन मिश्र और राजा दिनेश सिंह जेपी से मिलने सोखो देवरा आश्रम गए। वहां जेपी ने आचार्य राममूर्ति को भी बुलाया था। वहां लंबी बातचीत के बाद जेपी ने इंदिरा गांधी से मिलने पर अपनी सहमति दी। जेपी एक दिन पहले ही दिल्ली आए। वे गांधी शांति प्रतिष्ठान में ठहरे। वहां श्याम नंदन मिश्र जेपी से मिलने गए। जब बातचीत हो ही रही थी कि ‘जेपी के हाथ में एक पुर्जा आया। जिसे पढ़कर जेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दफ्तर से फोन आया है कि वे आपसे मिलना चाहती हैं।’
यह बात है, 31 अक्टूबर, 1974 की। श्याम नंदन मिश्र ने अपने लेख में यह लिखा है कि ‘इंदिरा गांधी जेपी का सामना करने से कतराती थी।’ लेकिन 1 नवंबर, 1974 को अंततः वार्ता हुई। उनके लेख में यह अंश सबसे अंत में है, ‘मुलाकात में इंदिरा जी के अलावा जगजीवन बाबू थे। जगजीवन बाबू ही ज्यादा बातें करते रहे।…अंत में इंदिरा जी ने जेपी से इतना ही कहा कि जयप्रकाश बाबू! जरा मुल्क के बारे में भी सोचिए। यह जेपी के लिए मार्मिक आघात था। जेपी ने वेदना भरी आवाज में उत्तर दिया–इंदु, और सारी जिंदगी मैंने किया क्या है?’ उस संवाद से विवादों का पिटारा खुलता ही चला गया।
